Bharat Muni ke natak se aap kya samajhte hain
भरतमुनि के नाटक से आप क्या समझते हैं?
विषय: इतिहास – भारतीय जीवन परंपरा | पेपर – I | विषय कोड: A3-HIST 1D)
✦ परिचय:
भारतीय साहित्य, कला और रंगमंच की परंपरा में भरतमुनि का योगदान अमूल्य और अद्वितीय है। उन्होंने लगभग 2000 वर्ष पूर्व ‘नाट्यशास्त्र’ की रचना की थी, जो दुनिया का सबसे प्राचीन नाट्यकला पर आधारित ग्रंथ है। भरतमुनि द्वारा रचित नाट्यशास्त्र में न केवल नाटक की शास्त्रीय परिभाषा दी गई है, बल्कि नृत्य, संगीत, अभिनय, मंच सज्जा, भाव-भंगिमा, भाषा, संवाद, वेशभूषा आदि की भी विस्तृत व्याख्या की गई है।
नाट्यशास्त्र में कुल 36 अध्याय और 6000 से अधिक श्लोक हैं, जिनमें नाटक को केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि समाज और धर्म का एक माध्यम बताया गया है। भरतमुनि के अनुसार, नाटक लोकानुरंजन, लोकशिक्षण और लोकसंग्रह का साधन है।
✦ भरतमुनि के नाटक की प्रमुख विशेषताएँ:
1. नाटक की परिभाषा और उद्देश्य:
भरतमुनि के अनुसार, नाटक जीवन का अनुकरण (Anukaran) है। इसमें व्यक्ति, समाज, धर्म, नीति, आचार, व्यवहार और जीवन की विविध स्थितियों का कलात्मक चित्रण होता है। नाटक का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि शिक्षा, उपदेश और चेतना का प्रसार करना है।
“नाट्यं भगवतो ब्रह्मणा लोकविनोदानाय धर्मार्थकाममोक्षाणां शिक्षार्थं कृतम्।”
– नाट्यशास्त्र
इसका अर्थ है कि नाटक धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जैसे पुरुषार्थों की शिक्षा देने हेतु बनाया गया है।
2. रस सिद्धांत (Rasa Theory):
भरतमुनि का रस सिद्धांत उनकी नाट्यचेतना की आत्मा है। उनके अनुसार, नाटक का मुख्य उद्देश्य है — दर्शकों में भावनाओं की उत्पत्ति करना, और अंततः एक विशेष “रस” का अनुभव कराना। भरतमुनि ने 8 प्रमुख रसों का उल्लेख किया:
-
श्रृंगार रस (प्रेम)
-
वीर रस (पराक्रम)
-
करुण रस (दया)
-
हास्य रस (हँसी)
-
रौद्र रस (क्रोध)
-
भयानक रस (डर)
-
बीभत्स रस (घृणा)
-
अद्भुत रस (आश्चर्य)
बाद में शांत रस को भी जोड़ा गया, जिससे रसों की संख्या 9 (नवरस) मानी गई।
इन रसों के माध्यम से नाटक दर्शक को जीवन की विविध अनुभूतियों से जोड़ता है और उसमें संवेदनशीलता, समझ और चेतना का विकास करता है।
3. पात्रों की संरचना (Characterization):
भरतमुनि ने नाटक में पात्रों को उनकी भूमिका, भाषा, स्वभाव और सामाजिक वर्ग के अनुसार विभाजित किया है। उन्होंने नायक, नायिका, विदूषक, खलनायक, मंत्री, सेवक आदि प्रकार के पात्रों का वर्णन किया है।
नायक को चार श्रेणियों में बाँटा गया:
-
धीरोदात्त (महान और आदर्श)
-
धीरप्रशांत (शांत और संयमी)
-
धीरललित (कोमल और विनोदी)
-
धीरशांत (तपस्वी प्रकृति का)
हर पात्र की भाषा, वेशभूषा और व्यवहार उसकी सामाजिक स्थिति के अनुरूप होती थी।
4. भाषा और संवाद:
नाटक में भाषा का प्रयोग पात्र की जाति, वर्ग, लिंग और स्तर के अनुसार होता था। भरतमुनि ने बताया कि:
-
उच्चवर्गीय पात्र संस्कृत में बोलते हैं।
-
मध्यमवर्ग या स्त्रियाँ प्राकृत में।
-
दास, सेवक, विदूषक आदि देशज भाषाओं का प्रयोग करते हैं।
संवादों में लय, छंद, मुहावरे और प्रतीकों का सुंदर प्रयोग किया जाता था, जिससे दृश्य और भाव अधिक प्रभावशाली बनते थे।
5. मंचन और अभिनय की विधियाँ:
भरतमुनि के नाट्यशास्त्र में अभिनय के तीन प्रकार बताए गए हैं:
-
आंगिक अभिनय: शरीर की मुद्राएँ और हाव-भाव
-
वाचिक अभिनय: संवाद, उच्चारण और स्वरों का प्रयोग
-
सात्त्विक अभिनय: अंतर्मन के भावों की अभिव्यक्ति (जैसे अश्रु, कम्पन, पसीना आदि)
साथ ही उन्होंने नेत्र, मुख, हाथ, पाँव, गर्दन आदि अंगों की विशेष मुद्राओं का वर्णन किया है। नाट्यशास्त्र में मंच की सज्जा, रंगों का प्रयोग, प्रकाश व्यवस्था, पार्श्व संगीत, प्रवेश और निकास आदि के नियम भी दिए गए हैं।
✦ भरतमुनि के नाटक से आधुनिक शिक्षा के लिए शिक्षाएँ:
-
समाज का दर्पण: नाटक समाज की अच्छाई और बुराई दोनों को प्रस्तुत करता है, जिससे विद्यार्थी सामाजिक समस्याओं को समझ सकते हैं।
-
सांस्कृतिक संरक्षण: नाटक के माध्यम से प्राचीन भारतीय मूल्यों, परंपराओं और लोकाचार का संरक्षण होता है।
-
रचनात्मक विकास: नाटक विद्यार्थियों में भाषा, अभिनय, अभिव्यक्ति, संवाद कला और नेतृत्व क्षमता को बढ़ाता है।
-
मानव मन की समझ: रस सिद्धांत के माध्यम से विद्यार्थी विभिन्न मनोवैज्ञानिक स्थितियों को समझना सीखते हैं।
✦ भरतमुनि के योगदान की आधुनिक प्रासंगिकता:
आज के डिजिटल युग, थिएटर, सिनेमा, टेलीविजन, और वेब सीरीज जैसे माध्यमों में भी भरतमुनि के सिद्धांतों की छाप देखी जा सकती है।
-
आज भी कलाकारों को भावाभिनय, संवाद, हाव-भाव, मंच सज्जा की शिक्षा दी जाती है, जो नाट्यशास्त्र में वर्णित है।
-
अभिनय विद्यालयों और नाट्य अकादमियों में भरतमुनि के सिद्धांतों को पढ़ाया जाता है।
इस प्रकार, भरतमुनि का योगदान केवल शास्त्रीय नाटक तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी अवधारणाएँ वर्तमान दृश्य माध्यमों में भी प्रभावी हैं।
✦ निष्कर्ष:
भरतमुनि का नाटक केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि यह शिक्षा, संस्कृति, धर्म, दर्शन और समाज सुधार का माध्यम है। उन्होंने नाटक को एक लोककल्याणकारी संस्था के रूप में प्रस्तुत किया।
नाट्यशास्त्र के माध्यम से भरतमुनि ने यह सिद्ध किया कि कला केवल आनंद का स्रोत नहीं, बल्कि एक गंभीर दार्शनिक, नैतिक और सामाजिक संरचना भी है।
यदि हम भरतमुनि के सिद्धांतों को समझें और अपनाएँ, तो शिक्षा और समाज दोनों में व्यापक परिवर्तन संभव है।
जैन धर्म के त्रिरत्न की व्याख्या कीजिए। Jain dharm ke Triratna ki vyakhya kijiye
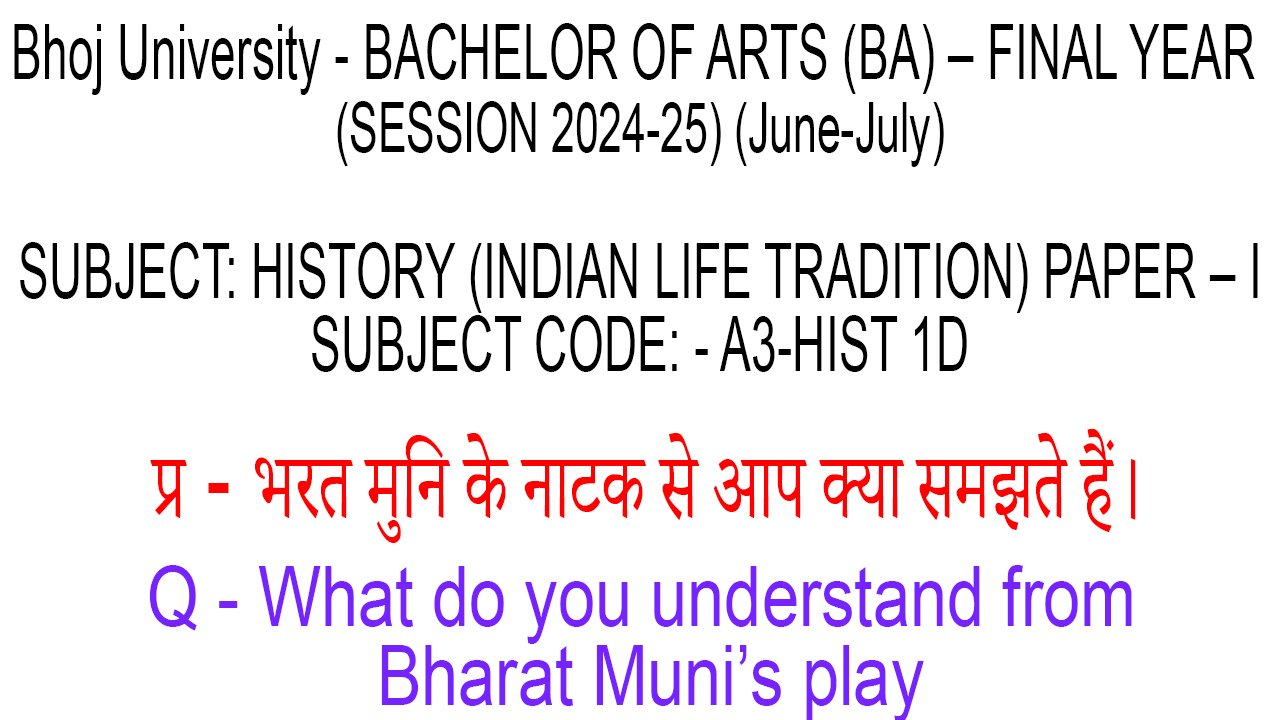
2 thoughts on “भरत मुनि के नाटक से आप क्या समझते हैं। Bharat Muni ke natak se aap kya samajhte hain”