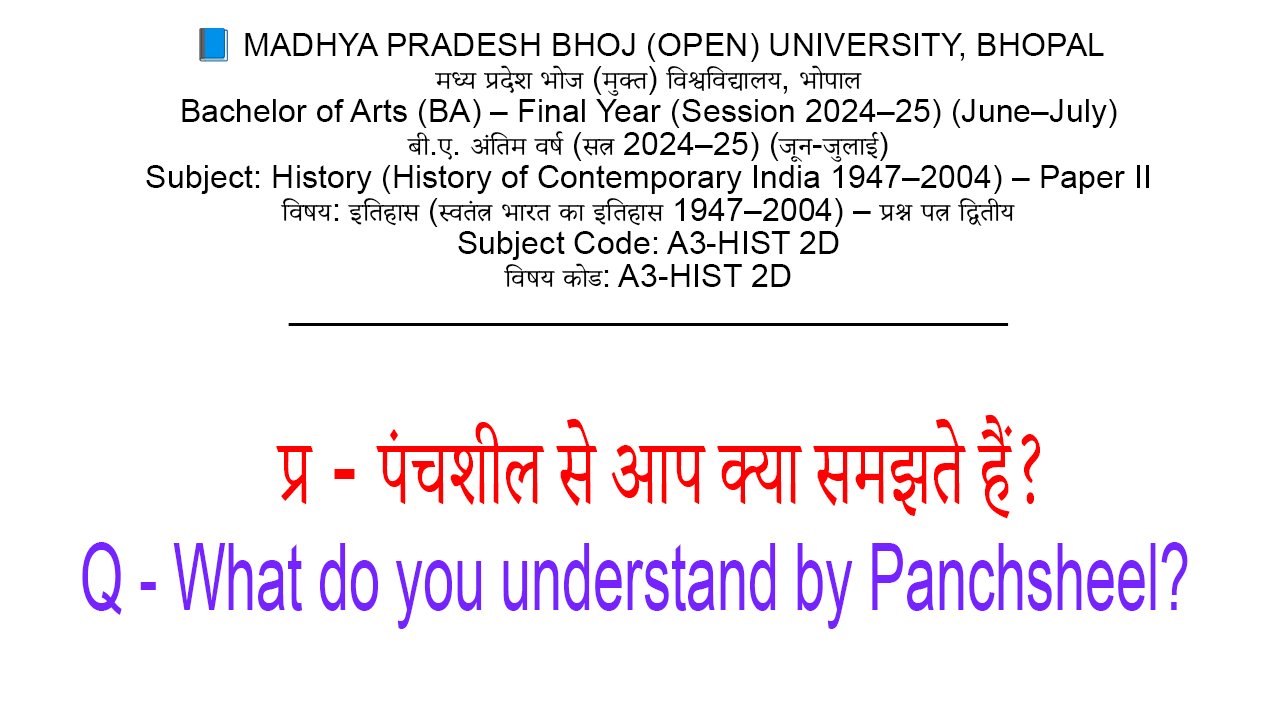Panchsheel se aap kya samajhte hain
पंचशील से आप क्या समझते हैं?
भारत के स्वतंत्रता के बाद के इतिहास (1947–2004) में पंचशील एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत और नीति के रूप में उभर कर सामने आया। पंचशील, भारत की विदेश नीति का मूल आधार और शांति, सह-अस्तित्व तथा आपसी सम्मान का प्रतीक है। पंचशील के सिद्धांतों को 29 अप्रैल 1954 को भारत और चीन के बीच हस्ताक्षरित एक समझौते में औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया था। यह समझौता मुख्य रूप से भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाउ एनलाई की पहल पर हुआ था।
नीचे पंचशील और उससे संबंधित ऐतिहासिक महत्व का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है:
पंचशील का अर्थ और उत्पत्ति
‘पंचशील’ शब्द का अर्थ है – पाँच शील या पाँच सिद्धांत। यह पाँच मूलभूत सिद्धांत शांति, सहयोग और परस्पर सम्मान पर आधारित हैं। पंचशील का विचार पहली बार 1954 में भारत-चीन सीमा समझौते के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया। इस समझौते में दोनों देशों ने अपने संबंधों को शांतिपूर्ण ढंग से विकसित करने और आक्रामकता से दूर रहने पर बल दिया।
भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने पंचशील को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की दिशा में मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया।
पंचशील के पाँच सिद्धांत
पंचशील समझौते में निम्नलिखित पाँच सिद्धांतों का उल्लेख है:
- एक-दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना।
इसका अर्थ है कि कोई भी देश दूसरे देश की सीमाओं, संप्रभुता या स्वतंत्रता का उल्लंघन न करे। - एक-दूसरे पर आक्रमण न करना।
किसी भी परिस्थिति में हिंसा या आक्रमण का सहारा न लेना। - एक-दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना।
किसी भी देश को दूसरे देश की आंतरिक राजनीति या प्रशासनिक व्यवस्था में दखलंदाजी का अधिकार नहीं है। - समानता और आपसी लाभ के आधार पर कार्य करना।
दोनों देश किसी भी समझौते में समान भागीदार होंगे और एक-दूसरे का शोषण नहीं करेंगे। - शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व।
सभी देश अलग-अलग विचारधाराओं और व्यवस्थाओं के बावजूद आपसी शांति और मित्रता बनाए रखेंगे।
पंचशील का ऐतिहासिक महत्व
- पंचशील ने भारत की विदेश नीति को अहिंसा और शांति के सिद्धांतों पर आधारित करने में मदद की।
- 1955 में बांडुंग सम्मेलन (इंडोनेशिया) में पंचशील के सिद्धांतों को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली।
- एशिया और अफ्रीका के नवस्वतंत्र राष्ट्रों ने पंचशील को अपनी आपसी कूटनीति का आधार बनाया।
- पंचशील ने शीतयुद्ध की राजनीति में भारत को “असंपृक्त” (Non-Aligned Movement) की ओर अग्रसर किया।
पंचशील और भारत-चीन संबंध
यद्यपि 1954 में भारत-चीन ने पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए, लेकिन 1962 में हुए भारत-चीन युद्ध ने पंचशील की अवधारणा को चुनौती दी। चीन द्वारा पंचशील सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए भारत पर आक्रमण करना एक बड़ा झटका था। इसके बावजूद, भारत ने पंचशील की नीति को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शांति और सहयोग का आधार बनाए रखा।
पंचशील और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति
पंचशील केवल भारत-चीन संबंधों तक सीमित नहीं रहा। बाद में इसे कई देशों ने अपनाया। 1961 में बेलग्रेड (यूगोस्लाविया) में आयोजित असंपृक्त आंदोलन (NAM) के पहले सम्मेलन में पंचशील के सिद्धांतों को ही आधार बनाया गया। यह आंदोलन पंडित नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासिर, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति टिटो और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो जैसे नेताओं की पहल पर शुरू हुआ।
पंचशील के लाभ और सीमाएँ
लाभ:
- पंचशील ने भारत की विदेश नीति को नैतिक आधार दिया।
- इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि एक शांतिप्रिय राष्ट्र के रूप में स्थापित हुई।
- नवस्वतंत्र राष्ट्रों के बीच आपसी सहयोग और भाईचारे की भावना बढ़ी।
सीमाएँ:
- पंचशील सिद्धांतों का पालन सभी देशों ने ईमानदारी से नहीं किया।
- भारत-चीन युद्ध ने इस नीति की व्यावहारिकता पर प्रश्नचिह्न लगाया।
- अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति और हित की राजनीति अक्सर पंचशील को कमजोर करती रही।
निष्कर्ष
पंचशील भारत की विदेश नीति का एक आदर्शवादी और शांतिपूर्ण आधार है। यद्यपि इसके कार्यान्वयन में कई चुनौतियाँ आईं, फिर भी यह आज भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में प्रासंगिक है। पंचशील के सिद्धांत, विशेषकर शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और परस्पर सम्मान, आज भी वैश्विक शांति की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं।
भारतीय संविधान की विशेषताओं को समझाइए। Bhartiya Samvidhan ki Visheshataon ko Samjhaiye
जम्मू और कश्मीर के भारत में महत्व को समझाइए। Jammu aur Kashmir ke Bharat mein Mahatva ko Samjhaiye
भारत के राजनीतिक एकीकरण से आप क्या समझते हैं? Bharat ke Rajneetik Ekiakaran se aap kya samajhte hain
भारत में आतंकवाद को समझाइए। Bharat mein Aatankvaad ko Samjhaiye